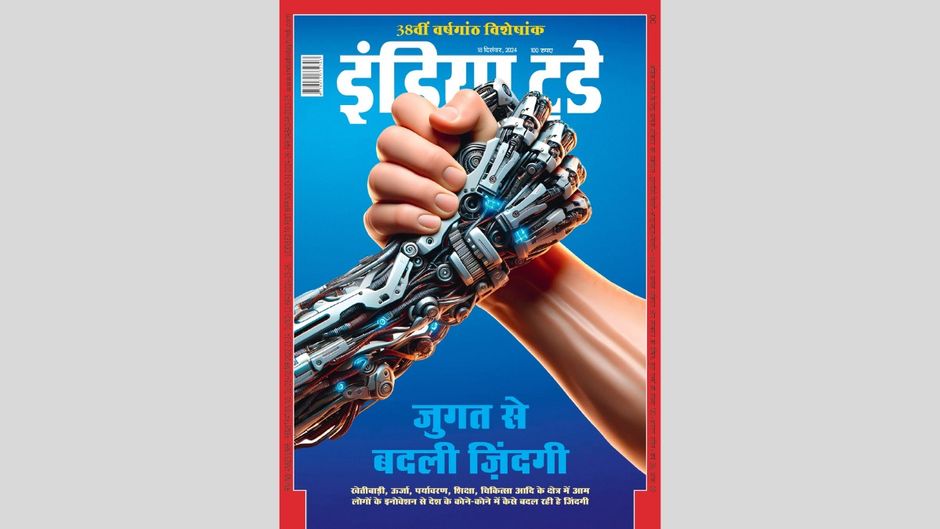—अरुण पुरी
मानव स्वभाव महत्वाकांक्षा और सुधार की आवश्यकता पर पनपता है. जरूरतें बढ़ने के साथ ही उसके समाधान भी विकसित हो जाते हैं. नवाचार और उद्यमशीलता की कोशिश ने इंसानी जिंदगी के हर पहलू में क्रांति ला दी है, जिससे यह अधिक सुविधाजनक और कुशल बन गया है. कृषि से लेकर अक्षय ऊर्जा तक, दवा से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक, भारत भर के नवोन्मेषक—चाहे वे व्यस्त शहरों में हों या अलसाए-से दूरदराज के गांवों में—मुश्किलों को आसान करने के तरीके निकाल रहे हैं.
1970 के दशक से पहले खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता हमें बेरहमी से याद दिलाती थी कि आत्मनिर्भरता क्या होती है. हरित क्रांति ने भारत को कृषि के लिहाज से स्वतंत्र राष्ट्र में बदलने में मदद की. भारत पिछले दशक में चुपचाप उस दौर में प्रवेश कर गया जिसे हरित क्रांति 2.0 कहा जा सकता है.
वैज्ञानिकों ने न केवल पैदावार बढ़ाई है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ विकल्प सुनिश्चित करते हुए उपज के पोषण मूल्य को भी बढ़ाया है. यह बदलाव पूरे देश में दिखाई दे रहा है. राजस्थान के रामनारायण थाकन ने पॉलीहाउस खेती और सर्दियों के दौरान ओस इकट्ठा करने जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देकर बसेड़ी गांव के किसानों को करोड़पति बना दिया है. उनके जैसे उदाहरण बताते हैं कि कैसे कृषि नवाचार समृद्धि और स्थिरता पैदा कर रहे हैं.
ऐसे व्यावहारिक समाधान ग्रामीण भारत में गहराई से गूंजते हैं, जहां संसाधन अक्सर कम होते हैं. सुलभ तकनीकों के साथ स्थानीय समस्याओं का समाधान करके स्थानीय किस्म के अन्वेषक न केवल जीवन को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान दे रहे हैं.
ऊर्जा नवाचार ने भी गति पकड़ी है, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में. बिहार के बर्निहार गांव में, आइआइटी-दिल्ली से प्रशिक्षित इंजीनियर विवेक प्रियदर्शी अपनी खुद की क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं. प्रियदर्शी गोबर के बायोगैस का उपयोग करके ट्रैक्टर, जीप और यहां तक कि क्रेन भी चलाते हैं. इसके अलावा, वे दूसरों को बायोगैस सिलेंडर भरने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो रही है और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है.
इस बीच, कानपुर के राहुल गुप्ता ने सौर पैनल तकनीक को बढ़ाया है, जिससे पैनल सूर्य की गति को ट्रैक करने में सक्षम हो गए हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. लखनऊ में पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह की 'नंदी ऊर्जा’ मशीन बैल की शक्ति का उपयोग करके प्रति घंटे 50 किलोवाट बिजली पैदा करती है. ये विविध नवाचार भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं.
स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिलचस्प पहलकदमियां देखने को मिली हैं. चिकित्सा संबंधी गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाया जा रहा है. मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक डॉक्टर फसलों में बैक्टीरिया, वायरल और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए होम्योपैथिक उपचार का उपयोग कर रहा है.
इस तरह के गैर-परंपरागत लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक नवाचार के बीच की खाई को पाटते हैं. बवासीर, फिशर और फिस्ट्यूला की समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर ने किफायती उपचार विधियां विकसित की हैं.
ये कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे तकनीक और नवाचार वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की बाधाओं को दूर कर सकते हैं. खासकर दीवाली के समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाना लंबे समय से वायु प्रदूषण का स्रोत रहा है. लेकिन गुजरात के जयेश पारीख ने पराली को एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया है. पारीख ने भूसे से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन निकालकर टायर, कागज, पेंट फिलर्स और यहां तक कि कार्बन फाइबर बनाने में इस्तेमाल होने वाली पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के लिए रास्ता तैयार किया है.
इस तरह के नवाचार न केवल पर्यावरण को राहत देते हैं बल्कि प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ किसानों के लिए आय के नए स्रोत भी बनाते हैं. वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसी तरह महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. कैशिफाइ के संस्थापक मंदीप मनोचा ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कचरे में तब्दील होने से रोका है. उनकी सफलता की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे इनोवेशन के जरिए बेकार पड़ी वस्तुओं को मूल्यवान संसाधनों में बदला जा सकता है.
नवोन्मेष प्रगति की रीढ़ है. ग्रामीण बिहार में धुआं रहित चूल्हों से लेकर बायोगैस से चलने वाले ट्रैक्टर और क्रांतिकारी चिकित्सा उपचारों तक, भारत के नवोन्मेषक रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ कारगर रास्ते निकाल रहे हैं. वे जीवन को आसान बना रहे, लागत कम कर रहे और स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं. इन सफलताओं के पीछे के बहुत-से चेहरे अक्सर मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं, जो यह बताते हैं कि नवोन्मेष केवल हाइ-टेक लैब या शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं.
इंडिया टुडे की 38वीं वर्षगांठ विशेषांक में विभिन्न क्षेत्रों के 27 नवोन्मेषकों के बारे में बताया गया है. प्रत्येक कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने और समाज को लाभ पहुंचाने वाले समाधान बनाने के लिए मानव के दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है. वे हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटे विचार में सार्थक बदलाव लाने की शक्ति होती है, बशर्ते इसे जुनून और एक मकसद के साथ आगे बढ़ाया जाए.
— अरुण पुरी, प्रधान संपादक और चेयरमैन (इंडिया टुडे समूह)