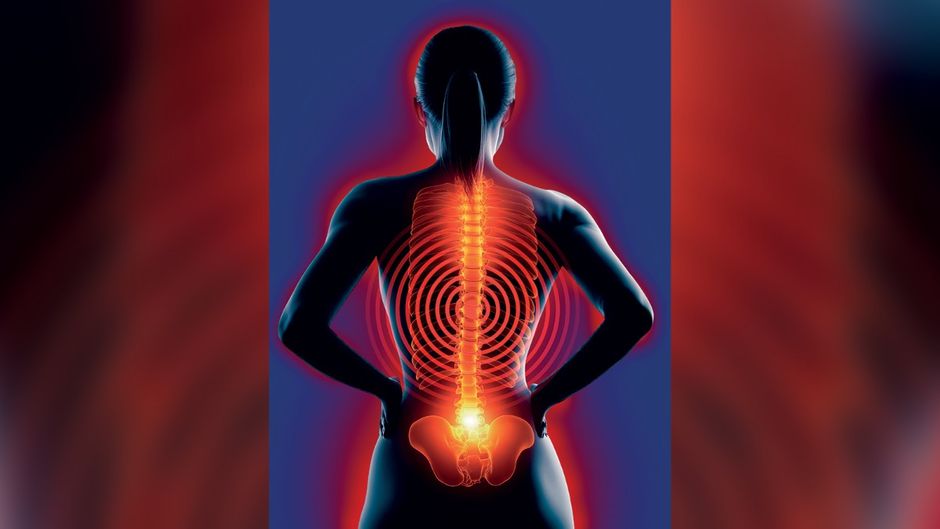उनतीस साल के रोहन मेहता ने कभी सोचा तक नहीं था कि इतनी कम उम्र में उन्हें स्लिप डिस्क जैसी दिक्कत होगी, जो आम तौर पर उम्रदराज लोगों को होती है. दिल्ली के उभरते डीजे रोहन ने लगातार रहने वाले कमर दर्द को बस खराब पोश्चर या बैठने के ढंग को समझकर नजरअंदाज कर दिया था. लेकिन जब एमआरआइ हुई, तो पता चला कि उन्हें स्लिप डिस्क है.
इसी वजह से कई हफ्तों से उनकी रातों की नींद हराम हो रखी थी और इतना दर्द था कि झुककर जूते के फीते बांधना भी मुश्किल हो गया था. डॉक्टरों ने बताया कि स्लिप डिस्क तब होती है जब रीढ़ की हड्डियों के बीच का नरम हिस्सा उभर आता है या फट जाता है, जिससे पास की नसों पर दबाव पड़ता है. लेकिन रोहन के लिए सबसे डराने वाला यह एहसास था कि उनकी रीढ़ की हड्डी उम्र से पहले ही बूढ़ी हो रही है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोहन की परेशानी किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि एक बड़ी ट्रेंड की झलक है. अब कमर और गर्दन का लगातार दर्द युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, और भारत भी उन देशों में शामिल हो रहा है जहां कमर दर्द के सबसे ज्यादा मामले हैं. घंटों कंप्यूटर पर झुककर काम करना, बैठे-बैठे दिन गुजारना और खराब वर्क सेटअप इस दिक्कत को और बढ़ा रहे हैं.
सिएटल के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स ऐंड इवैल्यूएशन की 2023 की 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज’ रिपोर्ट के मुताबिक, लोअर बैक पेन या कमर दर्द दुनिया भर में जल्दी मौत और सेहत बिगड़ने के आला 10 वजहों में एक है. इसी रिपोर्ट के 2021 वाले वर्जन में बताया गया था कि दुनिया भर में होने वाली रीढ़ की हड्डी की चोटों में 15 फीसद मामले भारत के हैं, जो चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा है. हाल ही में, 2025 में रिसर्चगेट में छपी एक स्टडी का अनुमान है कि भारत में करीब 15 लाख लोग रीढ़ की चोट की तकलीफ को लिए जी रहे हैं.
उससे भी चिंताजनक कम उम्र में इसका होना है. 2025 में क्योरियस: जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में छपी 18 राज्यों में 16,866 मरीजों की एक स्टडी में पता चला कि 2020 से 2023 के बीच कमर दर्द के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा मामले 18 से 38 साल के लोगों में है, यानी वह उम्र जब इंसान अपने करियर और काम के चरम पर होता है.
इसी तरह, 2024 में आइसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में छपी एक समीक्षा में खेती, स्वास्थ्य सेवा, खनन, बैंकिंग जैसे अलग-अलग सेक्टर में काम करने वालों पर हुए अध्ययनों को जोड़ा. नतीजा यह निकला कि पिछले एक साल में 60 फीसद कामकाजी लोगों में कमर दर्द की शिकायत थी.
आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन स्पाइन केयर अब एक नए मोड़ पर है. न्यूनतम चीर-फाड़ वाली सर्जरी, रोबोटिक्स और रीजनरेटिव थेरेपी जैसी नई तकनीक मरीजों को पहले से तेज रिकवरी, कम दर्द और कई मामलों में बिना सर्जरी के ठीक होने का मौका दे रही हैं. इन एडवांस तकनीकों के साथ योग और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होलिस्टिक थेरैपी जैसे इलाज मरीजों की ताकत और लचीलापन बढ़ाने में मदद कर रही हैं, जिससे रीढ़ की सेहत बनी रहती है. जो कभी आजीवन तकलीफ का नाम था, अब उसे संभाला जा सकता है, और कई बार पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है
कम उम्र में रोग
हम इंसानों की सबसे बड़ी खूबी सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता एक कीमत के साथ आई. जब इंसान चार पैरों से दो पैरों पर चलने लगा, तो रीढ़ की हड्डी ने अंग्रेजी अक्षर एस का आकार ले लिया. इससे हमारे हाथ आजाद हो गए, लेकिन शरीर पर नए तरह के दबाव आने लगे. यही वजह है कि रीढ़ जैविक रूप से उम्र के साथ घिसावट और टूट-फूट के लिए ज्यादा संवेदनशील हो गई. अब हमारी आधुनिक जीवनशैली इस प्राकृतिक गिरावट को और तेज कर रही है. रीढ़ की चोट गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हमेशा कमर में देखी जाती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, कमर दर्द दुनिया में अपंगता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. यह समस्या 2020 में 61.9 करोड़ लोगों में थी, लेकिन 2050 तक 84.3 करोड़ लोग इससे ग्रस्त हो सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादा एशिया के लोग होंगे. मामला गंभीर है, क्योंकि बेंगलूरू में ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर मणिपाल हॉस्पिटल्स के चेयरमैन तथा स्पाइन सर्जरी के प्रमुख डॉ. विद्यासागर एस. के मुताबिक, अगर किसी युवा को लगातार कमर दर्द रहता है, तो 40 वर्ष की उम्र तक उसके पुराने स्पाइन प्रॉब्लम में बदलने की 60 फीसद संभावना होती है. वे बताते हैं, ''कम उम्र में रीढ़ में विकृति डिस्क के जल्दी घिसने, समय से पहले गठिया, दर्द, सांस या नसों की समस्याओं का कारण बन सकती है.’’

कोयंबत्तूर के गंगा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा और स्पाइन सर्जरी विभाग के चेयरमैन तथा इंडियन स्पाइन जर्नल के एडिटर-इन-चीफ डॉ. एस. राजशेखरन भी इससे सहमत हैं, ''40 साल से कम उम्र के लोगों में रीढ़ और गर्दन के दर्द के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. अब 20 से 35 साल के युवाओं में भी डिस्क से जुड़ा पैर या हाथ का दर्द (जैसे सायटिका या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी) देखा जा रहा है.’’ यानी शिकायतें अब पहले से ज्यादा पेचीदा हो गई हैं.
चिंता सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर ही नहीं जता रहे हैं. बेंगलूरू के होलिस्टिक हेल्थ सेंटर सौक्या के फाउंडर डॉ. आइजाक मथाई कहते हैं, ''युवाओं में बढ़ती रीढ़ की दिक्कतों को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनाना चाहिए. शारीरिक लापरवाही और लगातार बढ़ता मानसिक तनाव मिलकर ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो पहले से कहीं जल्दी स्पाइनल दिक्कतों की शिकार हो रही है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग देर तक इलाज नहीं कराते, जिससे छोटी और आसानी से ठीक होने वाली परेशानियां धीरे-धीरे क्रॉनिक बन जाती हैं.’’
टीस जहां से उठती है
शरीर की बनावट में रीढ़ की हड्डी सबसे जटिल हिस्सों में है. यह न सिर्फ हमारे शरीर का स्तंभ है, बल्कि नसों का हाइवे भी है. इसकी जुड़ी हुई हड्डियां स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती हैं, जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने का मुख्य रास्ता है. इसलिए जब यहां कोई दिक्कत होती है, तो उसका असर चलने-फिरने, नसों के खिंचाव और रोजमर्रा के कामों पर बरसों तक रह सकता है.
रीढ़ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है सर्वाइकल स्पाइन, यानी गर्दन. यह बेहद लचीला होता है और सिर को संतुलित रखने और घुमाने-झुकाने में मदद करता है. लेकिन घंटों स्क्रीन पर झुके रहना, किसी झटके से गर्दन का झुक जाना या उम्र के साथ होने वाली जकड़न, यह सब इसकी लचक पर भारी पड़ते हैं. नतीजा यह होता है कि गर्दन अकड़ जाती है, दर्द कंधों और बाहों तक फैलने लगता है, और कभी-कभी सिरदर्द भी इसी वजह से शुरू होता है, जो सिर के निचले हिस्से से ऊपर तक चढ़ता है.
सर्वाइकल स्पाइन के बाद आता है थोरेसिक रीजन, यानी ऊपरी और बीच का पीठ वाला हिस्सा, जो हमारी पसलियों को सहारा देता है. यह हिस्सा शरीर को स्थिर रखने के लिए बना है, ज्यादा मूवमेंट के लिए नहीं. लेकिन झुक कर बैठने की आदत, कमजोर मांसपेशियां या हड्डियों का पतलापन इस हिस्से पर लगातार दबाव डालते हैं. यहां होने वाला दर्द अक्सर कंधों के बीच महसूस होता है या पसलियों के चारों ओर फैल सकता है, जिससे यह दिल या फेफड़ों की बीमारी जैसा लगता है.
इसके नीचे होता है लंबर स्पाइन, यानी कमर का निचला हिस्सा, जो शरीर का असली वर्कहॉर्स या सबसे उपयोगी हिस्सा है. यह हमारे शरीर का ज्यादातर वजन उठाता है और हर रोज के झटकों को झेलता है. इसलिए यही वह जगह है जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमर दर्द के मामले मिलते हैं. यहां मांसपेशियों में खिंचाव, डिस्क का बाहर निकलना या गठिया जैसी समस्याएं सुबह की अकडऩ से लेकर पैरों तक फैलने वाले तेज सायटिका दर्द तक का कारण बन सकती हैं.
रीढ़ के सबसे नीचे होता है सैक्रम और कॉकसिक्स—ये तिकोनी हड्डियां होती हैं जो पेल्विस (कूल्हे) से जुड़कर रीढ़ का आखिरी सिरा बनाती हैं, जिसे आम बोलचाल में टेलबोन या पूंछ की हड्डी कहते हैं. आम तौर पर इस हिस्से पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर गिरने से चोट लग जाए या लंबे समय तक सख्त कुर्सी पर बैठना पड़े, तो यहां बहुत तेज दर्द उठ सकता है जो काफी परेशान कर देता है.
जोखिम के कारक
कई लोगों में शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, पढ़ाई के लंबे सत्रों के बाद कंधों में जकड़न, गर्दन के नीचे लगातार बना रहने वाला दर्द या थकान जो आराम के बाद भी ठीक नहीं होती. फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. आशीष तोमर के मुताबिक, आज की लाइफस्टाइल ''युवाओं की रीढ़ की बनावट धीरे-धीरे बदल रही है’’, और ये बदलाव अब किशोरों में भी दिखने लगे हैं.
आंकड़े भी यही बताते हैं. जर्नल ऑफ बॉडीवर्क ऐंड मूवमेंट थेरैपीज में 2024 में प्रकाशित पूरे भारत के 8वीं से 12वीं क्लास के 1,007 छात्रों की एक स्टडी में 61 फीसद ने बताया कि ई-लर्निंग डिवाइस इस्तेमाल करने से उनकी गर्दन में दर्द रहता है. मुंबई की गृहिणी नेहा शर्मा के लिए यह चिंता घर तक पहुंच गई, जब उनके 11 साल के बेटे को सिर पीछे झुकाने में दिक्कत होने लगी. डॉक्टर ने बताया कि यह ई-लर्निग और लगातार गेम खेलने की वजह से गर्दन की गलत पोजिशन का असर है.
नेहा कहती हैं, ''वह हमेशा आगे झुका रहता है, पढ़ाई हो या मोबाइल स्क्रीन. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में बच्चे को ऐसी तकलीफ हो सकती है.’’ इसी तरह जर्नल ऑफ फार्मेसी ऐंड बायोएलाइड साइंसेज में 2024 में छपे एक और रिसर्च में 500 भारतीय स्कूली बच्चों में पाया गया कि उनके बैग का औसत वजन उनके शरीर के वजन का करीब 13.5 फीसद था. नतीजतन, आधे लड़कों और लगभग दो-तिहाई लड़कियों ने बताया कि उन्हें कमर दर्द की समस्या रहती है.
ऑफिस का काम भी कम सजा नहीं देता. पुणे के 24 साल के डिजाइन इंटर्न सुरेश राघवन को घर से काम शुरू किए बस छह महीने ही हुए थे कि उनकी पीठ में दर्द शुरू हो गया. वजहें साफ थीं: डायनिंग चेयर को ऑफिस चेयर की तरह इस्तेमाल करना, लैपटॉप को बहुत नीचे रखना और बिना ब्रेक लिए घंटों काम करना. सुरेश याद करते हैं, ''दिन खत्म होते-होते कंधे पत्थर जैसे लगने लगते थे.’’
एक्स-रे कराने पर पता चला कि उन्हें शुरुआती पोश्चरल काइफोसिस है, यानी रीढ़ की ऊपरी हड्डी का आगे की ओर झुक जाना. इसे आजकल आम भाषा में 'टेक नेक’ कहा जाता है, जो लगातार स्क्रीन पर झुके रहने से होता है. डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह झुकाव हमेशा के लिए स्थायी हो सकता है. उसका अनुभव 2025 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ऐंड इनोवेटिव रिसर्च में छपी एक स्टडी से मेल खाता है, जिसमें बताया गया कि पश्चिम भारत में कॉर्पोरेट डेस्क वर्क करने वाले 300 लोगों (22 से 40 वर्ष उम्र) को गर्दन के दर्द की समस्या है.
मोटापा इस परेशानी में एक और परत जोड़ देता है. ज्यादा वजन रीढ़ की हड्डियों और जोड़ों पर ज्यादा दबाव डालता है, और मांसपेशियों की कमजोरी और सूजन दर्द को और बढ़ा देती है. इसमें पोषण का असर भी अहम होता है, लेकिन अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं. विटामिन डी की कमी से हड्डियां मुलायम पड़ जाती हैं, जबकि मैग्नीशियम की कमी से कैल्शियम ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता.
चेन्नै की 22 साल की आॢकटेक्चर छात्रा काव्या मेनन को इसका एहसास महंगी कीमत चुकाकर हुआ. वे ज्यादातर प्रोसेस्ड स्नैक्स खाती थीं और घर के बाहर की गतिविधियों से दूर रहती थीं. उन्हें शुरुआती ऑस्टियोमलेशिया का पता चला. यह ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां मजबूती खोने लगती हैं क्योंकि उनमें खनिज ठीक से नहीं जमते. काव्या बताती हैं, ''पहले तो लगा कि यह सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस है, बाद में पता चला कि मेरी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थीं.’’
एक्सपर्ट्स का कहना है कि तनाव शायद सबसे कम आंका गया कारण है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक ऐंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में 2024 में छपे एक स्टडी में भारतीय मेडिकल छात्रों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि कमर दर्द के मामले बहुत आम हैं और यह तनाव, लंबे समय तक बैठे रहने की आदत और गलत बॉडी पोश्चर से जुड़े हैं. मसलन, एम्स जोधपुर में तीन में चार मेडिकल छात्रों ने बताया कि उन्हें पिछले दो साल में कम से कम एक बार कमर दर्द हुआ, जबकि 41.8 फीसद छात्रों को पिछले चार हक्रतों में ही दर्द हुआ था.
जो हाल मेडिकल छात्रों का है, वही ऊंचे हलके के पेशेवरों का है. डॉ. मथाई बताते हैं, ''लगातार स्ट्रेस से गर्दन, कंधों और कमर की मांसपेशियां हमेशा तन जाती हैं.’’ समय के साथ ये गलत पोश्चर बना देता है, नसों पर दबाव डालता है, चलने-फिरने की क्षमता घटाता है और कुछ मामलों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस (गर्दन की हड्डियों का समय से पहले घिस जाना) और क्रोनिक कमर दर्द जैसी गंभीर दिक्कतें पैदा कर देता है.
रीढ़ इलाज के नए तरीके
दशकों से चले आ रहे रीढ़ की देखभाल के तरीके अब पहले जैसे नहीं रहे. अगर किसी को स्लिप डिस्क या तेज कमर दर्द होता था, तो आम सलाह होती थी: आराम करो, वह भी हफ्तों तक. लेकिन अब डॉक्टर मानते हैं कि यह तरीका उल्टा नुक्सान पहुंचा सकता है. लंबे समय तक बिना हरकत रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जकड़न बढ़ जाती है और रिकवरी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. अब डॉक्टर मरीजों को जल्दी ऐक्टिव होने को कहते हैं. हल्की-फुल्की फिजियोथेरैपी से मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन दोबारा बनाने पर जोर दिया जाता है, ताकि शरीर अपनी सामान्य चाल और सहनशक्ति वापस पा सके.
यही सोच अब पुराने इलाजों पर भी लागू हो रही है. पहले लंबे समय तक चलने वाले कमर दर्द में बड़े-बड़े बैक ब्रेस या कॉर्सेट पहनने की सलाह आम थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ खास मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, टीनएजर्स में स्कोलियोसिस (रीढ़ की हड्डी का तिरछा झुकाव) या कुछ सर्जरी के बाद. रिसर्च बताती है कि ये उपकरण लंबे समय तक राहत नहीं देते. इसी तरह, गर्दन और कमर के दर्द में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्शन अब पुराना तरीका माना जाता है.
इससे थोड़ी देर के लिए दर्द कम तो हो सकता है, लेकिन असली कारण पर असर नहीं पड़ता. आधुनिक सर्जरी तकनीकों के आने के बाद उसकी जरूरत लगभग खत्म हो चुकी है. यहां तक कि स्पाइनल इंजेक्शन—खासकर बार-बार दिए जाने वाले एपिड्यूरल स्टेरॉयड शॉट्स—पर भी अब दोबारा विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये राहत तो देते हैं लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, और इनके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं. इनकी जगह अब नई बायोलॉजिकल थेरेपीज और ज्यादा सटीक, टार्गेटेड ट्रीटमेंट धीरे-धीरे जगह बना रहे हैं, जिनमें दर्द को सिर्फ दबाने पर नहीं बल्कि जड़ से ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है.
स्पाइन केयर में सबसे बड़ा बदलाव मिनिमली इनवेसिव सर्जरी (एमआइएस) के आने से हुआ है. पहले जहां रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने के लिए मांसपेशियों को बड़े हिस्से में काटना पड़ता था, अब सर्जन छोटी-छोटी जगहों से यानी की-होल सर्जरी के जरिए अंदर पहुंच सकते हैं. पतले औजारों और कैमरे की मदद से वे स्लिप डिस्क ठीक कर सकते हैं, स्कोलियोसिस सीधी कर सकते हैं या हड्डियों को स्थिर कर सकते हैं.

एमआइएस-टीएलआइएफ (ट्रांसफॉर्मेशनल लंबर इंटरबॉडी क्रयूजन) और एमआइएस-पीएलआइएफ (पोस्टीरियर लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन) जैसी तकनीक इसी बदलाव के उदाहरण हैं. आसान भाषा में कहें तो इसमें खराब डिस्क को निकालकर उसकी जगह बोन ग्राक्रट लगाया जाता है ताकि आसपास की हड्डियां एक साथ जुड़ जाएं और ये सब दो सेंटीमीटर से भी छोटी चीरे से किया जा सकता है. सर्जरी का खर्च करीब 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पड़ सकता है.
गुरुग्राम में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूरोसर्जरी विभाग के हेड और एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. संदीप वैश्य कहते हैं, ''पिछले दो-तीन दशकों में टेक्नोलॉजी ने कमाल की तरक्की की है.’’ वे बताते हैं कि अब स्पाइन इम्प्लांट के साथ-साथ सर्जरी के दौरान इंट्रा-ऑपरेटिव सीटी और एमआरआइ स्कैन का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो डॉक्टरों को ऑपरेशन के वक्त ही रीढ़ की हड्डी की रियल-टाइम इमेज दिखाते हैं. इसके अलावा, न्यूरो-नेविगेशन सिस्टम, जिसे आप दिमाग के लिए जीपीएस कह सकते हैं, सर्जनों को बेहद सटीकता से स्क्रू लगाने में मदद करते हैं. वे बताते हैं, ''अब कई सर्जरी तो लोकल एनेस्थीसिया देकर भी की जा सकती हैं और मरीज अगले ही दिन चलकर घर जा सकता है.’’
अब रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) ने स्पाइन सर्जरी की सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया है. गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑर्थो-स्पाइन सर्जरी विभाग के हेड डॉ. हितेश गर्ग कहते हैं, ''पिछले दस साल में स्पाइन सर्जरी में ऐसे बदलाव आए हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.’’
वे बताते हैं कि रोबोट-असिस्टेड सिस्टम्स में सर्जन रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जो मिलीमीटर स्तर की सटीकता से स्क्रू और इम्प्लांट लगाते हैं. इससे नर्व को नुक्सान पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक होते हैं. वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी सर्जनों को ऑपरेशन के दौरान शरीर की अंदरूनी बनावट का डिजिटल ओवरले दिखाती है, जैसे कोई रियल-टाइम एक्स-रे विजर हो. हालांकि यह टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं है.
रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की कीमत करीब 4 से 9 लाख रुपए तक होती है, जबकि एआर वाली सर्जरी ज्यादा महंगी पड़ सकती है.
इन सबके पीछे नई तरह के इम्प्लांट का भी योगदान है, जैसे 3डी-प्रिंटेड टाइटेनियम केजेज और एक्सपैंडेबल स्पेसर्स. ये ज्यादा मजबूत, शरीर के अनुकूल और हर मरीज की शारीरिक बनावट के हिसाब से बनाए जा सकते हैं. मरीजों के लिए इसका मतलब है अस्पताल में कम रहना, छोटे निशान और सामान्य जिंदगी में जल्दी वापसी.
नतीजे वाकई चमत्कारी होते हैं. दिल्ली के साकेत में मैक्स हेल्थकेयर, न्यूरोसर्जरी और न्यूरोस्पाइन विभाग के चेयरमैन और हेड डॉ. बिपिन वालिया कहते हैं, ''नई मिनिमल-एक्सेस सर्जरी के नतीजे पारंपरिक सर्जरी जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कट बहुत छोटे होते हैं, टिश्यू को कम नुक्सान होता है, खून की जरूरत कम पड़ती है और सबसे अहम रिकवरी जल्दी होती है.’’ वे एक केस का जिक्र करते हैं: एक युवती खेलते वक्त हुए हादसे में गर्दन से नीचे तक पैरालाइज हो गई थी. डॉ. वालिया बताते हैं, ''सर्जरी के महीने के भीतर वह फिर से चलने लगी. तीन महीने में वह पूरी तरह ऐक्टिव हो गर्ई और राष्ट्रपति के हाथों स्पोर्ट्स अवॉर्ड भी मिला.’’
सर्जरी अब पहले से कहीं कम इनवेसिव हो गई है. स्पाइन के इलाज में रीजनरेटिव मेडिसिन के साथ ही एक और फ्यूचरिस्टिक बदलाव शुरू हो चुका है. इसका मकसद है खराब हो चुके डिस्क को निकालने या जोड़ने के बजाए उन्हें खुद से ठीक करना. इस दिशा में दो तरीके चर्चा में हैं: स्टेम सेल थेरैपी और प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (पीआरपी) इंजेक्शन.
स्टेम सेल्स हमारे शरीर की खास रिपेयर सेल्स होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर अलग-अलग तरह के टिश्यू में बदल सकती हैं. स्टेम सेल्स ट्रांसलेशनल मेडिसिन नाम की एक हालिया मल्टी-सेंटर स्टडी में पाया गया कि जब बोन मैरो या फैट से ली गई मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स को खराब हो चुके स्पाइनल डिस्क में इंजेक्ट किया गया, तो मरीजों के दर्द में दो साल के भीतर करीब 70 फीसद तक कमी आई. इसी तरह द स्पाइन जर्नल में प्रकाशित एक मेटा-एनालिसिस के मुताबिक, पीआरपी—जिसे आम तौर पर स्पोर्ट्स इंजरीज में हीलिंग तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है—क्रोनिक लोअर बैक पेन कम करने में भी असरदार साबित हो रहा है.
भारत में कई प्राइवेट सेंटर अब इन नई थेरैपीज पर काम कर रहे हैं. मुंबई का न्यूरोजेन ब्रेन ऐंड स्पाइन इंस्टीट्यूट खुद को न्यूरोलॉजिकल और स्पाइनल डिसऑर्डर के लिए सेल थेरेपी में लीडर मानता है, जबकि स्पाइन सर्जरी इंडिया कई सेंटर पर स्टेम सेल ट्रीटमेंट के ऑप्शन देता है. दिल्ली का रीजेन ऑर्थो स्पोर्ट रीजनरेटिव स्पाइन ट्रीटमेंट को स्टेम सेल कॉन्सन्ट्रेट्स के जरिए प्रमोट कर रहा है.
वहीं, टोश ट्रॉमा ऐंड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल (चेन्नै) और स्टेमसेलकेयरइंडिया (दिल्ली) जैसे सेंटर भी डिस्क डिजेनरेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए स्टेम सेल-आधारित इलाज ऑफर करते हैं. इन ट्रीटमेंट की कीमत एक साइकल के लिए आम तौर पर 3 लाख से 8 लाख रुपए तक होती है. इसके साथ ही पीआरपी थेरैपी का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है. दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर इसे स्लिप डिस्क और क्रोनिक बैक पेन के लिए ऑफर करता है. मैक्स हेल्थकेयर इसे मस्क्युलोस्केलेटल और स्पाइन से जुड़ी दिक्कतों के लिए प्रमोट करता है. इसका खर्च अमूमन 10,000 से 30,000 रुपए प्रति सिटिंग के बीच होता है.
हालांकि, डॉक्टर इन थेरैपीज को लेकर सावधान भी करते हैं. स्टेम सेल और पीआरपी थेरैपी अभी भी प्रयोग के स्तर में हैं, और नतीजे हर मरीज और तरीके के हिसाब से अलग हो सकते हैं. दीर्घकालिक डेटा बहुत कम है, इलाज महंगा है और रेगुलेशन भी स्पष्ट नहीं है. कुछ क्लिनिक इन अनप्रूव्ड ट्रीटमेंट को सर्जरी से बचने वाले मरीजों को बेच रहे हैं.
होलिस्टिक वेलनेस की ओर
भारत अब अपनी पारंपरिक विधियों से भी रास्ता निकाल रहा है. आयुर्वेदिक विधियां जैसे कटि बस्ती में गर्म दवा वाला तेल कमर पर डालकर दर्द और जकड़न कम की जाती है और पिझिचिल में पूरे शरीर पर गर्म हर्बल तेल डालकर मालिश की जाती है. पंचकर्म में मसाज, हर्बल ट्रीटमेंट और शरीर की गहराई से सफाई के पांच मुख्य उपाय शामिल होते हैं. इसका उद्देश्य शरीर में सूजन कम करना और नेचुरल हीलिंग को बढ़ावा देना होता है.
योग को भी अब स्पाइन केयर के लिए नए तरीके से अपनाया जा रहा है, जैसे डिजिटल डिटॉक्स योग टेक नेक यानी लगातार स्क्रीन झुककर देखने से होने वाली तकलीफ को कम करता है, वॉल रोप योग रीढ़ को सेफ तरीके से स्ट्रेच करता है, और आयंगर योगा थेरैप में बेल्ट, बोल्स्टर और प्रॉप्स की मदद से बॉडी अलाइनमेंट और ताकत दोबारा बहाल की जाती है.
पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर में शरीर के खास बिंदुओं पर पतली सुइयां लगाई जाती हैं, अब रीहैब प्रोग्राम का अहम हिस्सा बनती जा रही है. नई दिल्ली में सर गंगा राम हॉस्पिटल, में हेड ऑफ एक्यूपंक्चर डॉ. रमन कपूर कहते हैं, ''यह हड्डियों को दोबारा सीधा नहीं कर सकती, लेकिन यह मसल्स को रिलैक्स, ब्लड प्लो को बेहतर और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने में मदद करती है.’’
लेकिन कई बार सेहत के पीछे भागना उल्टा पड़ सकता है. महामारी के दौरान 28 साल की दिल्ली निवासी प्रिया मल्होत्रा ने बिना किसी ट्रेनर की निगरानी के ऑनलाइन योग ट्यूटोरियल्स फॉलो करना शुरू किया. जैसे-जैसे उन्होंने एडवांस्ड बैकबेंड्स और ट्विस्ट्स करने की कोशिश की, उनकी कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द शुरू हो गया. वे बताती हैं, ''मुझे लगा योग तो सेफ होता है, मैंने दर्द को नजरअंदाज कर दिया.’’ लेकिन एमआरआइ हुई, तो पता चला कि उनकी लंबर स्पाइन में स्ट्रेन और डिस्क में शुरुआती बदलाव आ चुके हैं. वे कई महीनों की फिजियोथेरेपी और गाइडेड ट्रेनिंग के बाद ही ठीक हो पाईं.
ऐसी गलतियों से बचने के लिए डॉ. कपूर कहते हैं, ''कोई एक परफेक्ट पोश्चर नहीं होता. असल बात है एक डायनेमिक और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाना, जिससे रीढ़ हमेशा सपोर्टेड, स्ट्रॉन्ग और क्रलेक्सिबल बनी रहे.’’ डॉ. मथाई होलिस्टिक एप्रोच की सलाह देते हैं.
नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज टास्कफोर्स ऑन स्पाइन केयर के चेयरमैन डॉ. छाबड़ा का मानना है कि नीति स्तर पर देशभर में डब्ल्यूएचओ की 2023 के क्रॉनिक लो बैक पेन के दिशानिर्देशों को अपनाना ज़रूरी है. जागरूकता, नीतिगत सुधार और मेडिकल इनोवेशन मिलकर भारत में स्पाइन केयर को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं. जो कभी छुपी हुई दर्द की महामारी थी, वह अब प्रोएक्टिव हेल्थ, सुलभ इलाज और लंबी, सेहतमंद जिंदगी का मॉडल बन सकती है.