आवरण कथाः गैर-बराबरी का राजकाज
तरक्की के मौकों तक पहुंच के मामले में गैर-बराबरी देश की विकास के सफर को नुकसान पहुंचाएगी, 'भारत निर्माण' के लिए हमें 'भारत सुशासन' की नई अवधारणा पर काम करना होगा.
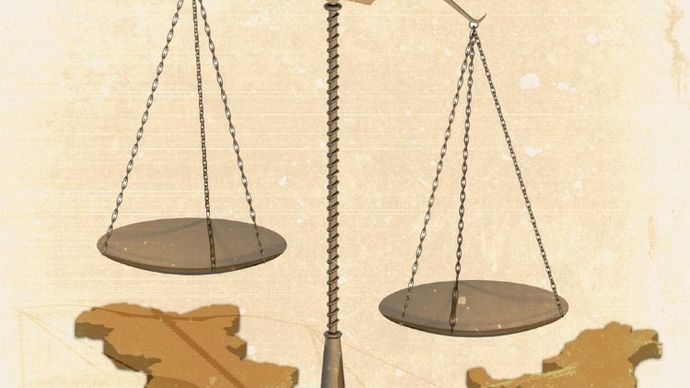
असमानता पर नई दिल्ली में होने वाली नीतिगत बहसें गरीबी, लगातार गिरते गिनी सूचकांक ('भारतीय आय असमानता, 1922- 2014'' लुकास चांसेल और थॉमस पिकेट्टी) पर केंद्रित होती हैं या फिर इस पर कि कैसे ऊपर के 1 फीसदी लोगों ने राष्ट्रीय आमदनी के 22 फीसदी हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है जबकि निचले आधे हिस्से के खाते में सिर्फ 15 फीसदी आता है. (विश्व असमानता रिपोर्ट 2017). लेकिन सड़क पर जुलूस-जलसे में उतरे लोग गैर-बराबरी को अवसरों की असमानता के रूप में देखते हैं.
यह बात वाकई पते की लगती है. सालाना महज 1,710 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय (जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 57,000 डॉलर और चीन में 8,100 डॉलर है) से साफ संकेत मिलता है कि अभी हमें विकास की दिशा में लंबा सफर तय करना है. हमारी असली संपदा यानी 18 साल से कम उम्र के 45 करोड़ नागरिकों को अभी अपने सफर की शुरुआत करनी है. उनके लिए (बाजार, सेवाओं और स्थान के मामले में) बढ़ते मौकों तक उनकी पहुंच की मात्रा ही गैर-बराबरी मापने का पैमाना हो सकती है. लेकिन, जब ज्यादातर जानकार जोरशोर से दावा कर रहे हैं कि 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर से हमारी सारी दिक्कतें छू मंतर हो जाएंगी, तो भला गैर-बरारबरी पर चिंता करने की जरूरत क्या है?
गैर-बराबरी कर सकती है विकास की रफ्तार अवरुद्घ
तमाम विकसित देश यह कोशिश करते हैं कि उनेयहां लगातार उत्पादक वृद्घि दर बनी रहे. ऐसा लगता है कि यह वृद्धि कुलमिलाकर व्यक्तियों के साथ समाज को भी फायइदा पहुंचाती है. विकास को दीर्घावधिक और टिकाऊ दो कारक बनाते हैं: लगातार सामाजिक गतिशीलता और हर आदमी का उससे जुड़ाव. विकास का वृत्त हर व्यक्ति को समान रूप से और एक साथ लाभ नहीं पहुंचाता. अक्सर ऐसा स्वाभाविक बढ़त में फर्क से होता है जैसे कोई समुदाय कितना पढ़ा-लिखा है, या बंदरगाहों या उपजाऊ भूमि तक उसकी पहुंच कितनी है, वगैरह. या फिर सरकारी पूंजी के आवंटन से भी अंतर पैदा हो सकता है, जैसे सड़कों के बदले हवाईअड्डों में निवेश, सिंचाई पर ध्यान हो या पुलिस बल पर, कोई विकासोन्मुखी नेता चुना जाए या किसी समझौते से उपजा उम्मीदवार.
कारण जो भी हों लेकिन हकीकत यही है कि लोग विकास के अलग-अलग रास्तों को चुनते हैं. फिर उन्हें यह भी यकीन दिलाना चाहिए कि उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है. उन्हें यह भरोसा करना पड़ता है कि एक दिन उन्हें भी मौका मिलेगा. वरना असंतोष की ध्वनियां विरोध में तब्दील हो जाती हैं. अगर उन्हें सुना नहीं जाता है तो लोग 'कोई और' खड़ा कर लेते हैं और अतिरेक वाले राजनैतिक विकल्पों के पक्ष में वोट देकर समूची व्यवस्था को ही खारिज कर देते हैं. ब्रेक्जिट और ट्रंप इसके दो उदाहरण हैं. तो, क्या सभी भारतीय यह मानते हैं कि अवसरों, जगहों और सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान है?
बुनियादी सेवाएं और सब्सिडी अवसर मुहैया होना नहीं
पहले अच्छी खबर. सत्तर साल के लोकतंत्र ने सदियों से गैर-बराबरी पर आधारित सभ्यता में एक नया आयाम जो दिया है कि हर भारतीय जन्म से बराबर है. राज्य की कोशिशों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, सबको स्कूल में दाखिला, दुनिया का सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण सड़कें और, अब सबके लिए बिजली और सुलभ आवास. हमारी भारी आबादी और क्षेत्र के मद्देनजर ये सब आसान काम नहीं.
तो, चुनौती क्या है? ये सरकारी उपाय बराबरी कायम करने के लिए काफी नहीं हैं.
हर युवा को अवसरों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उसे स्वस्थ, हुनरमंद होना चाहिए और उसे ऐसे समुदाय से होना चाहिए जिसमें नीतियों की वजह से उसके हुनर और उम्मीदों के अनुसार पर्याप्त रोजगार अवसर (निजी या सरकारी) पैदा होते हों. हकीकत यह है कि मातृ सेहत और साफ-सफाई की बदहाली से तकरीबन 48 फीसदी बच्चों का विकास रुक जाता है. अपर्याप्त ढांचे और उपयुक्त अध्यापक प्रशिक्षण के अभाव में 40 फीसदी बच्चे आठवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते स्कूल छोड़ देते हैं,12 फीसदी से भी कम युवा ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर पाते हैं. उसके बाद उनकी पढ़ाई और हुनर उनकी नौकरियों से मेल नहीं खाते.
निर्माण, सेवा-सत्कार, और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार तो पैदा करेंगे लेकिन हम उन रोजगारों के लिए लोगों को कुशल नहीं बना रहे (या सामाजिक समानता पैदा नहीं कर रहे). और, अंत में हमारी नीतियां विकास की सकारात्मक दिशा में नहीं, बल्कि अक्सर आसान राह चुन लेती हैं. हाल में जाटों, मराठाओं, पाटीदारों और कापुओं के आंदोलन हुए जो कभी संपन्न और राजनैतिक रूप से प्रभावशाली तबके रहे हैं. उन्हें अपने समुदायों के शिक्षित युवाओं को लेकर चिंता है क्योंकि सरकारी नौकरियां 'आरक्षित' हैं और निजी नौकरियां बहुत कम हैं. उनके लिए सार्वजनिक नौकरियों की उम्मीद खड़ी करना एक समाधान हो सकता है लेकिन उन्हें अच्छी नौकरियां या रोजगार चाहिए, चाहे कृषि में हों या फिर शहरों में.
कृषि को फायदेमंद बनाने के लिए बड़ा बदलाव की दरकार होगीः प्रौद्योगिकीय निवेश, विस्तृत भू-इस्तेमाल (भू-स्वामित्व नहीं), फसलों में बदलाव और उपज कीमतों पर ताकतवर बिचैलियों के दबदबे का खात्मा. इन सारे सख्त विकल्पों के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिए. लेकिन हमारे नेताओं को तो कृषि ऋण की माफी सबसे आसान समाधान नजर आती है.
इसी तरह भारतीय महिलाओं के मामले में अवसर बेहद कम हैं. 900 स्त्री-पुरुष अनुपात और मात्र 27 फीसदी कामकाजी महिलाएं (पश्चिम एशिया को छोड़ दें तो समूची दुनिया में सबसे निम्न स्तर) बताती हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए जगह कितनी कम है. जिस देश में लाखों की संख्या में डॉक्टरों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और उद्यमियों की जरूरत है वहां तो यह इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की प्रतिभा को गंवा देने जैसा है. इसी तरह सुरक्षा के खातिर घर के भीतर कैद रहने से शहरी युवाओं को मोटापा घेर रहा है.
21वीं सदी में भी अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाहों को जगह नहीं मिल रही है और निरापद प्रेम को नफरत की फिजा में जेहाद बता दिया जाता है. अंत में, नागरिक सेवाओं तक पहुंच सीमित ही बनी रहती है. आपूर्ति की खासी तंगी वाले तीन क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासन) का भारत की कोर मुद्रास्फीति में 37 फीसदी योगदान है जो भारत को इस मायने में अनूठा बनाता है कि उसकी राजकोषीय नीति ही उसकी मौद्रिक नीति को भी तय करती है.
इसका ऐतिहासिक समाधान एक दो स्तर वाला बाजार रहा है. संपन्न और ताकतवर वर्ग निजी बाजार तक पहुंच रखता रहा है या फिर उसे सार्वजनिक संपत्ति की वरीयता पर उपलब्धता रही है. गरीबों को या तो ज्यादा भुगतान करना पड़ता रहा है या फिर उन्हें सेवा में अंतर को बरदाश्त करना पड़ा है. स्कूल में एडमिशन से लेकर अस्पताल में बिस्तर तक के लिए उन्हें दर-दर की खाक छाननी पड़ती है. लेकिन ऐसा आगे नहीं चल पाएगा. हमारी राजनैतिक कार्यप्रणाली को आधिक पारदर्शी बनाना होगा.
सुधार का मंत्र ऊपर से नीचे तक लोकतंत्र
दो कारक मददगार हो सकते हैं. एकदम निचले स्तर तक लोकतंत्र का विस्तार हो और राजकाज का नजरिया बदले. राजनैतिक दलों ने चुनावों को जीतने के लिए नए बिजनेस मॉडल के साथ प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं. इसमें लोगों से सीधा संवाद, स्थानीय इलाकों के अनुरूप संदेश तैयार करना, और वोटिंग बूथों का प्रबंधन प्रमुख है, ताकि आखिरी सिरे तक मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा सके.
जल्द ही स्मार्ट मतदाता नतीजों की अपेक्षा रखेंगे. जागरूक मतदाता टेक्नोलॉजी और अपेक्षाओं के जरिए नीतियों और पूंजी आवंटित करने के लिए पसंद-नापसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीचे से आने वाला लोकतंत्र आखिरकार ऊपर से थोपे जाने वाले नेताओं की परिपाटी को तोड़ सकता है. 2018 में कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और इनमें हम युवाओं को उम्मीदवारों और पार्टियों के सामने ज्यादा अपेक्षाएं रखते देख सकते हैं.
राजनैतिक नेता जरूरी हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं. भारत को सक्रिय, उन्नत नागरिक संस्थानों की जरूरत है जो समाज के संरक्षक बन सकें, व्यवसाय और राज्य के बीच ईमानदार बिचैलियों की भूमिका निभा सकें और यह आश्वस्त कर सकें कि लोग अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में सचेत रहें. ऐसी पहल की शुरुआत के लिए 2018 अच्छा साल है, क्योंकि इस बार लाखों की संख्या में पहली बार वोट देने वाले भी हैं.
भारतीय लोग अमीरों से घृणा नहीं करते. यकीनन, संपन्न बनना अक्सर उनके सपनों का हिस्सा होता है. लेकिन वे इस बात को महसूस करना नहीं चाहते कि अमीरों और राजनैतिक नेताओं ने (इनमें अमूमन मिलीभगत रहती है) उनके खेल में फर्जीवाड़ा कर दिया है. वे यह यकीन करना चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास भी कामयाब होने के मौके हों. तरक्की के अवसरों की उपलब्धता में गैर-बराबरी ही भारत के विकास की कहानी को नुक्सान पहुंचा सकती है. कुशल नेता इस बात को आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे कि यह खेल ईमानदारी से खेला जाए. वरना भारत की विकास कहानी वक्त से पहले ही खत्म हो सकती है.
इरीना विट्टल मैकिंजे की पूर्व पार्टनर हैं और भारत में शहरीकरण और कृषि पर काफी काम कर चुकी हैं

